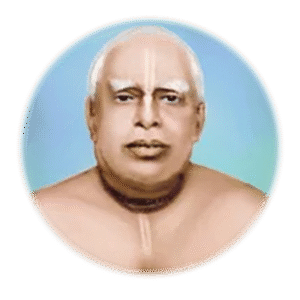
जिसे पवित्र जैवधर्म कहा जाता है, उसका ही दूसरा नाम वैष्णव धर्म है। जीव का जो सनातन स्वभाव धर्म है, उसी को ‘जैवधर्म’ कहा जाता है। जब जीव सभी उपाधियों से मुक्त हो जाता है, तब उसका स्वरूप शुद्ध, चिन्मय और प्रेममय होता है। उस अवस्था में उसका धर्म होता है — बिना किसी उपाधि के परम प्रेम। किन्तु जब वह जीव जड़ रूपी बंधन से युक्त होता है, तब उसका वह प्रेम विकृत हो जाता है, और उसमें जड़ उपाधियों का मिश्रण हो जाता है। शुद्ध जीव का जो वैष्णव धर्म है, वह बंधनयुक्त जीव में विकृत रूप में प्रकट होता है।
बंधनयुक्त जीव जड़ शरीर में आबद्ध होकर जड़ विधान के अधीन हो जाता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जितने प्रकार के नियम हैं, वे सभी जड़ की दृष्टि से होते हैं। यदि जीव को अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति करनी है, तो उसे इन जड़ संबंधों को त्यागना होगा। लेकिन यह त्याग सहसा संभव नहीं है। जड़ शरीर में रहते हुए ही उसे जड़ता से मुक्ति के लिए योग्य उपायों का सहारा लेना होगा। यह सोचकर कि जड़ संबंध अच्छे नहीं हैं, शरीर को नष्ट कर देना कोई लाभ नहीं देगा; बल्कि वह आत्मघात रूप पाप होगा जिससे और भी बंधन उत्पन्न हो सकता है। अतः जो जीव अपने स्वरूप की प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए शरीर की रक्षा आवश्यक है — केवल रक्षा ही नहीं, शरीर के पोषण, वृद्धि और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी प्रयत्न करना जरूरी है।
यदि शरीर को ठीक प्रकार से चलाना है, तो जीविका का कोई निष्पाप उपाय अपनाना भी आवश्यक है। और उस निष्पाप जीवन निर्वाह के लिए एक आश्रम और गृहस्थी का संकल्प लेना भी उचित है। चाहे कोई गृहस्थ के रूप में जीवन यापन करे या ब्रह्मचर्य अथवा संन्यास ग्रहण करे, उसे किसी न किसी आश्रम में अवश्य रहना चाहिए। और आश्रम के अनुसार एक उपयुक्त समाज का भी निर्माण करना होगा। इस प्रकार विषयासक्तों, मुक्ति की इच्छा रखने वालों तथा मुक्त आत्माओं — इन तीनों के लिए भिन्न-भिन्न समाज होते हैं।
कुछ लोग यह मानते हैं कि जो समाजिक है, वह वैष्णव नहीं हो सकता। यह एक भ्रम है। वस्तुतः समाज तीन प्रकार के होते हैं — विषयासक्त समाज, मुमुक्षु समाज और मुक्त समाज। जीव कभी भी समाज से अलग नहीं होता। जीव का स्वभाव ही समाजशील है। यहाँ तक कि जड़ता से मुक्त होने पर भी जीव का शुद्ध भक्ति-समाज आवश्यक होता है। अतः चाहे वन में रहो या वैकुण्ठ में — जीव सदा समाज से जुड़ा होता है। वैष्णव जीव और सामान्य जीव में यही अंतर है कि एक का समाज वैष्णव समाज होता है और दूसरे का सामान्य या विषयासक्त समाज।
इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैष्णव धर्म और वैष्णव समाज में कोई भेद नहीं है।
वैष्णव समाज और अन्य समाजों में अंतर यह है कि वैष्णव समाज का एकमात्र परम उद्देश्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, जबकि अन्य समाजों का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत कामना की पूर्ति। अन्य समाजों के लोग शरीर की पुष्टि, इन्द्रियों की तृप्ति, नीति और भौतिक विज्ञान की चर्चा को ही जीवन और समाज का परम उद्देश्य मानते हैं। कोई मरणोपरांत सुख को प्राथमिकता देता है, कोई स्वर्गीय भोग को, और कोई आत्मा की समाप्ति को ही सर्वोच्च मानता है।
वहीं दूसरी ओर, वैष्णव समाज में रहने वाले जीव शरीर की देखभाल, इन्द्रिय संयम, विज्ञान और नीति को भगवान के प्रेम की साधना के लिए सहायक मानते हैं। देखने में दोनों समाज एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव और उद्देश्य भिन्न होता है।
जो लोग समाज-शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वे एक स्वर से यह स्वीकार करते हैं कि वर्णाश्रम-व्यवस्था ही सर्वोत्तम सामाजिक व्यवस्था है। जब जीव वर्णाश्रम धर्म में स्थित होता है, तब उसकी मूल प्रकृति नष्ट नहीं होती, बल्कि उसे भगवान की प्रेम भक्ति के लिए अवसर और सुविधा प्राप्त होती है।
वर्णाश्रम धर्म ही बंधन में पड़े जीवों के लिए एकमात्र उपयुक्त समाज व्यवस्था है। वर्णाश्रम धर्म क्या है, इसका विस्तार से वर्णन ‘श्रीचैतन्य शिक्षामृत’ के पहले और दूसरे अध्याय में किया गया है। इसलिए यहाँ उसका पूरा विश्लेषण नहीं किया जा रहा, केवल इतना जानना आवश्यक है कि मनुष्य को अपने स्वभाववश एक वर्ण और अपनी स्थिति अनुसार एक आश्रम स्वीकार कर, जीवन निर्वाह करते हुए भगवान को प्रसन्न करना चाहिए।
कई प्रकार के कर्म और घटनाओं के माध्यम से स्वभाव का निर्माण होता है, जिनमें जन्म भी एक घटना है। लेकिन आज के समय में केवल जन्म को ही वर्ण का निर्धारक मानने से वर्णाश्रम धर्म पतित हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उस धर्म में स्थित लोग भी अपने कर्मों में सफल नहीं हो पाते। वर्णाश्रम धर्म की इस स्थिति को देखकर बहुत से सहृदयजन भारत के भविष्य को लेकर निराश हो गए हैं। इसी कारण अनेक विद्वान लोग वर्णधर्म की पुनः स्थापना के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि वर्ण धर्म के विनाश से संसार का कल्याण नहीं हो सकता। वर्णधर्म ही सामाजिक मानव का मूल जीवन रूप है। वर्णाश्रम का नाश हो जाने से मानव का वैज्ञानिक समाज नष्ट हो जाएगा। तब मनुष्य फिर से नीच अवस्था को प्राप्त होकर स्वेच्छाचारी और विधि-विहीन जीवन जीने लगेगा। इसीलिए किसी भी देशभक्त का उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म को नष्ट करना नहीं हो सकता। केवल इसमें जो मलिनता आ गई है, उसे ही दूर करना आवश्यक है।
यदि वर्णाश्रम धर्म को फिर से उसके स्वाभाविक रूप में लाना है, तो कुछ आवश्यक नियमों और सिद्धांतों को पुनः समाज में स्थापित करना होगा।
1. केवल जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति का वर्ण निश्चित नहीं किया जाना चाहिए।
2. बाल्यकाल की संगति और ज्ञान संग्रह के अनुसार जिसमें जो स्वभाव प्रबल रूप से प्रकट होता है, उसी के अनुसार उस व्यक्ति का वर्ण निर्धारित किया जाना चाहिए।
3. वर्ण निर्धारण करते समय स्वभाव और रुचि के साथ-साथ माता-पिता के वर्ण को भी कुछ हद तक ध्यान में रखना चाहिए।
4. जब कोई बालक उपयुक्त आयु — लगभग 15 वर्ष — को प्राप्त कर ले, तब कुल पुरोहित, भू-स्वामी, माता-पिता और गाँव के कुछ निष्पक्ष विद्वान मिलकर उसका वर्ण निर्धारण करें।
5. बाल्यावस्था पार कर चुके पुरुष के विषय में यह नहीं पूछा जाएगा कि उसका क्या वर्ण होना चाहिए, बल्कि यह देखा जाएगा कि क्या वह अपने पितृ-वर्ण की योग्यताओं को प्राप्त कर चुका है।
6. यदि देखा जाए कि वह पितृवर्ण के योग्य है, तो उसी के अनुसार उसका संस्कार किया जाएगा। यदि वह उच्च वर्ण का अधिकारी बन चुका है, तो उसे उसी के अनुसार संस्कारित किया जाएगा। यदि वह निम्न वर्ण के योग्य पाया जाता है, तो उसे दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी।
7. दो वर्षों के पश्चात फिर से उसका परीक्षण करके वर्ण निर्धारित किया जाएगा।
8. प्रत्येक गाँव में भू-स्वामियों और पंडितों द्वारा एक समाज-संरक्षक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।
9. इन सभी कार्यों को उचित रीति से लागू करने के लिए सम्राट (शासक) का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। सम्राट ही वर्णाश्रम धर्म के वास्तविक रक्षक होते हैं।
10. प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुरूप ही विवाह आदि संस्कारों तथा अधिकारों की अनुमति होनी चाहिए। जो व्यक्ति इससे भिन्न आचरण करे, उसे राज्यदंड दिया जाना चाहिए।
अब प्रश्न उठता है — क्या आज के युग में ऐसी समाज-संरचना संभव है? हमारी दृष्टि में इसका सहज रूप से होना कठिन है।
पहली बात, शासकीय सहयोग प्राप्त होना कठिन है।
दूसरी बात, यदि वह सहयोग मिल भी जाए, तो जब तक शासक स्वयं वर्णाश्रम धर्म को न अपनाएं, तब तक उनके द्वारा निष्पक्ष सहयोग मिलना असंभव है।
जहाँ तक आम जनता की बात है, भारतवासियों से भी इस विषय में पूर्ण सहयोग की आशा नहीं की जा सकती। स्वार्थवश बहुत से लोग इस आवश्यक सुधार के विरुद्ध होंगे। और सुधार के समय अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करेंगे। निम्न वर्ण के लोग भी अज्ञान और मूर्खता के कारण वर्तमान कुप्रथाओं को सहसा त्याग नहीं कर पाएंगे।
अतः कुछ सहृदय व्यक्ति मिलकर भी इस महान कार्य को तुरंत संपन्न नहीं कर सकते।
अब स्थिति यह है कि दोनों ही मार्गों में बाधा है। एक ओर कुप्रथा समाज को निर्बल बना रही है, दूसरी ओर यदि हम उसे सुधारने का प्रयत्न नहीं करें, तो केवल अमंगल ही प्राप्त होगा।
जिस आर्य वंश की तेजस्विता से एक समय संपूर्ण पृथ्वी काँपती थी, उसी आर्य संतान आज म्लेच्छों से भी अधिक अधम होती जा रही है।
जिनके हृदय में संवेदना है, वे इन बातों को सुनकर रो रहे हैं। और जिनके हृदय शून्य हैं, वे निश्चिंत भाव से अधोगति की ओर जा रहे हैं।
अब यदि हम वर्णाश्रम व्यवस्था को त्याग कर कोई नई व्यवस्था स्थापित करें, तो हम अपने आर्यत्व को खो देंगे, क्योंकि वैज्ञानिक समाज-रचना का नाश हो जाएगा।
इतिहास साक्षी है कि बौद्ध, जैन, ख्रिस्तीय, ब्रह्म समाज जैसी वर्णाश्रम-विहीन व्यवस्थाएँ भारत में कभी स्थिर नहीं हो सकीं। वे या तो पहाड़ों की गुफाओं में छिप गईं, या विदेशियों की कृपा पर जीवित रहीं, या केवल घरों के अंदर सिमट गईं।
अब प्रश्न है — उपाय क्या है? आवश्यकता है केवल मंगल की। परंतु वह मंगल कैसे सहज रूप से प्राप्त हो, यही विचार करना चाहिए।
जब तक वर्णाश्रम धर्म शुद्ध होकर वास्तविक स्वरूप में नहीं आता, तब तक सामाजिक, आध्यात्मिक और परमार्थिक अमंगल हमारे ऊपर मंडराते रहेंगे।
परंतु सारे मंगल का मूल स्रोत स्वयं भगवान ही हैं। वही समस्त संकटों का निवारण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।
कुछ लोग पुराणों के आधार पर मानते हैं कि कलियुग के अंत में श्रीकंधिदेव अवतीर्ण होकर मरु और देवापि नामक राजाओं की सहायता से वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, और उसी से सतयुग का आरंभ होगा।
किन्तु हम कहते हैं — यह सामान्य कलियुग नहीं है। इसे पूर्व के महापुरुषों ने ‘धन्य कलियुग’ कहा है। सामान्य कलियुग में ही कलिकाल के अंत में धर्म की पुनः स्थापना होती है।
परंतु इस धन्य कलियुग में स्वयं परिपूर्ण शक्तिमान, परम करुणामय, प्रेममूर्ति श्रीचैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हो चुके हैं।
इसलिए इस कलियुग में क्या संदेह? उस करुणामय महाप्रभु की कृपा से शीघ्र ही समस्त सामाजिक अमंगल दूर हो जाएगा।
यदि हम निष्कपट भाव से उनके चरणों में आश्रय लें, तो फिर किसी अन्य उपाय की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।
भगवद्भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है।
श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध में कहा गया है कि परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसके विपरीत, जो लोग सांसारिक सुख, भोग, ऐश्वर्य आदि सांसारिक फलों की प्राप्ति चाहते हैं, वे विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। ऐसे लोग बर्णाश्रम-धर्म के भीतर रहते हुए अनेक देवताओं और कर्मकांडों के शरणागत होते हैं।
परंतु यदि कोई जीव इस संसार में रहते हुए समस्त देवताओं का परित्याग कर केवल एकमात्र अच्युत भगवान के शरण में जा सके, तब ही उसे “परिनिष्ठित” की संज्ञा दी जाती है।
इस अवस्था का लक्षण भागवत में इस प्रकार कहा गया है—
“अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः।
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्।।” (भाग. २.३.१०)
इस संसार के सभी प्राणी “सर्वकाम” अर्थात अनेक इच्छाओं से युक्त हैं। फिर भी यदि वे उन इच्छाओं की पूर्ति हेतु विविध देवताओं की पूजा न करके केवल सर्वोच्च पुरुष की तीव्र भक्ति से उपासना करें, तो ऐसे लोग सामान्य बर्णाश्रमियों की अपेक्षा उच्च माने जाते हैं — इसमें कोई संशय नहीं है।
लेकिन इस मार्ग में एक कठिनाई है — ‘तीव्रेण भक्तियोगेन’ — इस पद के अनुसार तीव्र भक्ति के बिना अच्युत भगवान की शरण में जाना सम्भव नहीं।
शाश्वत वेदसम्मत बर्णाश्रम-व्यवस्था में निष्कपटता से स्थित रहने पर मानव समाज निर्दोष बना रहता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति तीव्र भक्ति के बिना ही अच्युत-शरणता का दावा करे, तो वह दोनों स्थानों से गिर जाता है। न वह सही बर्णाश्रमी रहता है, न ही सही वैष्णव।
तीव्र भक्ति ही अच्युत कुल का वास्तविक जीवन है।
हमारा अभिप्राय यह है कि ‘गृहस्थ वैष्णव’ शब्द का अर्थ केवल बर्णाश्रमी वैष्णव ही नहीं, बल्कि परिनिष्ठित वैष्णव को भी सम्मिलित करता है। परंतु परिनिष्ठित गृहस्थ के लिए यह कठिनाई है कि यदि उसमें तीव्र भक्ति नहीं पाई जाती, तो वह दोनों कुलों से च्युत हो जाता है।
श्रीकृष्ण की भक्ति के लिए यदि कोई बर्णाश्रम का त्याग करता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि वह त्याग करके कृष्णभक्ति से भी दूर हो जाए, तो वह दोष का भागी बनता है। ऐसे व्यक्ति को ‘वैष्णव’ कहकर आदर नहीं किया जा सकता।
समाज के दृष्टिकोण से वैष्णव तीन प्रकार के होते हैं—
(1) सनिष्ठ — जो बर्णाश्रम में रहते हुए श्रीकृष्ण के भक्त हैं।
(2) परिनिष्ठित — जो कर्मकांड का त्याग कर केवल अच्युत भगवान के शरण में हैं, परंतु गृहस्थ हैं।
(3) निरपेक्ष — जो स्वरूपतः अपने स्वधर्म का भी त्याग कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में त्यागी होते हैं और गृहस्थ नहीं होते।
इन तीनों में भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है, लेकिन सभी के लिए कृष्णभक्ति ही जीवन है।
यदि किसी परिनिष्ठित या निरपेक्ष व्यक्ति की कृष्णभक्ति क्षीण हो जाए, तो उनका पतन स्वीकार करना ही होगा।
केवल बर्णाश्रम को स्वीकारना, या उसका त्याग कर लेना, अथवा विशेष वेश-भूषा धारण करना ही वैष्णवता नहीं है। वास्तविक वैष्णव वह है, जिसमें श्रीकृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति हो।
वैष्णव कहलाने के लिए आवश्यक मात्रा में कृष्णभक्ति होनी चाहिए — इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
एक और गूढ़ विषय यह है कि सनिष्ठ और परिनिष्ठित — दोनों ही गृहस्थ हैं। अतः वे कौपीन (संन्यास-चिह्न) धारण करने के अधिकारी नहीं हैं। जिसके पास अधिकार नहीं, यदि वह ऐसे कार्य करे, तो वह पुण्य नहीं बल्कि दोष बन जाता है। सनिष्ठ वैष्णवों के लिए कृष्णमंत्र-ग्रहण ही वैष्णवता का बाह्य चिन्ह है। परिनिष्ठित व्यक्ति को पांच संस्कार (संन्यास दीक्षा के चिह्न) नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वे अभी भी बर्णाश्रम के भीतर ही हैं। निरपेक्ष व्यक्ति के लिए ही कौपीन धारण करना उचित है, वही उसका बाह्य वैष्णव चिन्ह बनता है। यह सभी शास्त्रों द्वारा सिद्ध है।
यदि कोई परिनिष्ठित व्यक्ति कौपीन धारण कर ले, तो वह अपराध करता है। कौपीन धारण करनेवाला फिर कभी स्त्रीसंग नहीं कर सकता। इसके असंख्य प्रमाण हैं। इसलिए परिनिष्ठित गृहस्थ वैष्णवों में जो धर्म-विरुद्ध कार्य दिखते हैं, उनका सुधार अत्यंत आवश्यक है। आज हमने यह विषय संक्षेप में प्रस्तुत किया। परिनिष्ठित गृहस्थों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए धन संचय करना आवश्यक है। लेकिन इस विषय में भी अनेक शास्त्रीय विचार हैं। यदि वे भागवत के सातवें स्कंध में उल्लिखित बर्णाश्रम धर्म को स्वीकार न करें, तो उन्हें भिक्षा द्वारा अपना पालन करना पड़ेगा। किन्तु भिक्षा का अधिकार केवल निरपेक्ष त्यागियों को ही है। इसलिए परिनिष्ठित गृहस्थों को अपने स्वभाव के अनुसार किसी उपयुक्त बर्ण का निर्धारण कर उसके अनुरूप कार्य करते हुए जीवन-निर्वाह करना चाहिए।
भागवत में कहा गया है—
“जिसमें जिस बर्ण के लक्षण पाए जाते हैं, उसे उसी बर्ण में माना जाए। केवल जन्म से किसी का बर्ण निश्चित नहीं होता।”
(भाग. ७.११.३५)